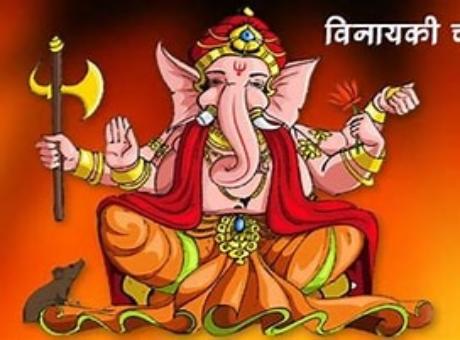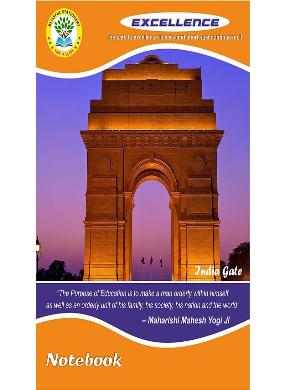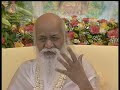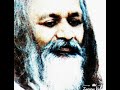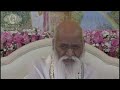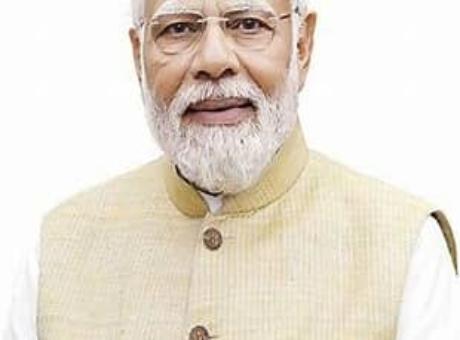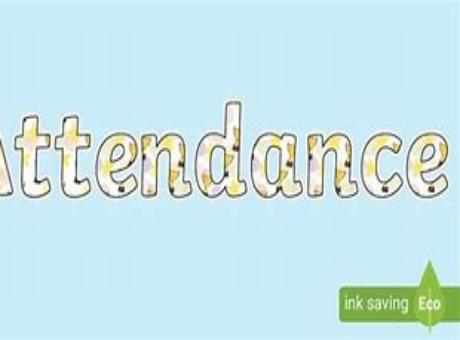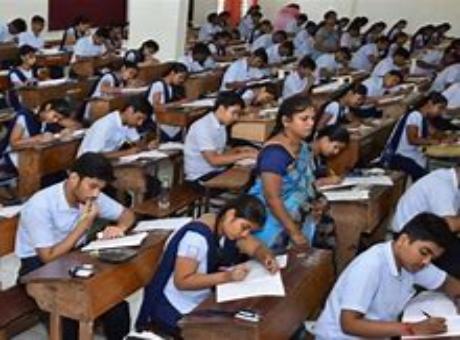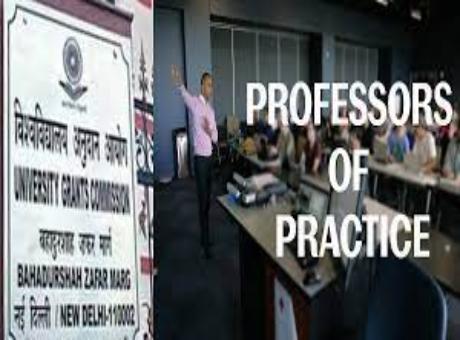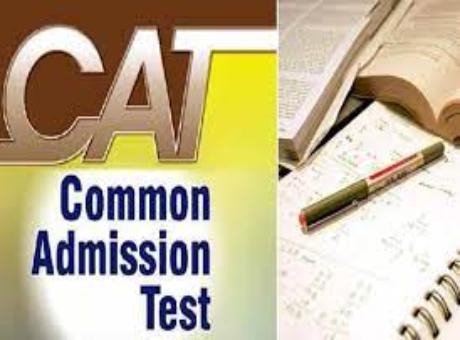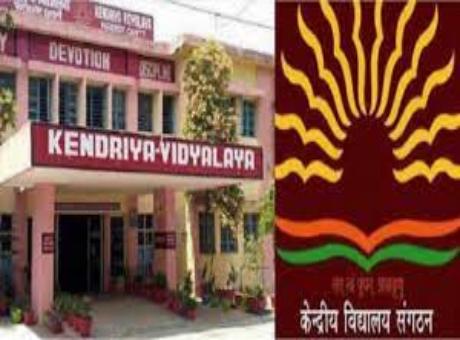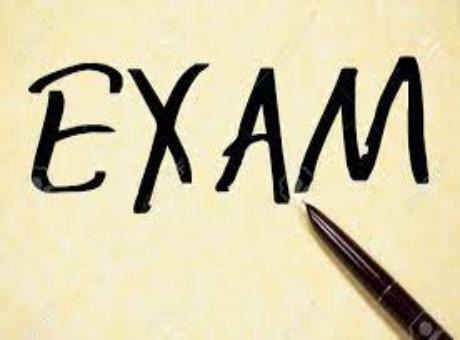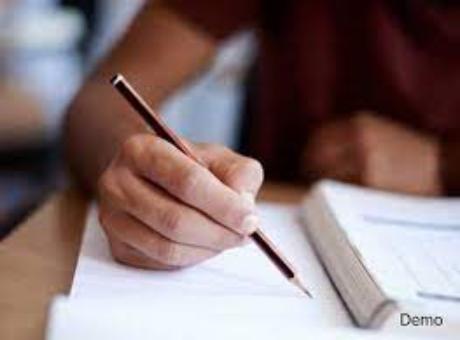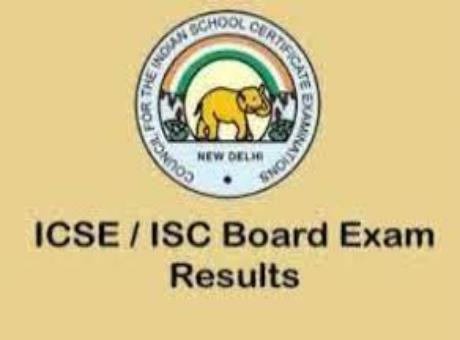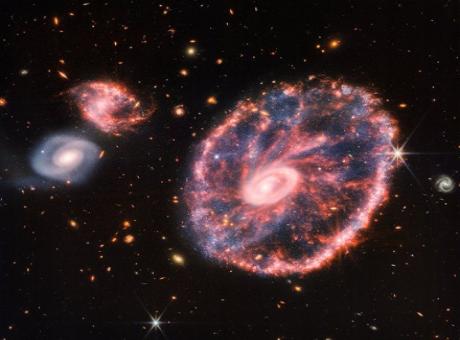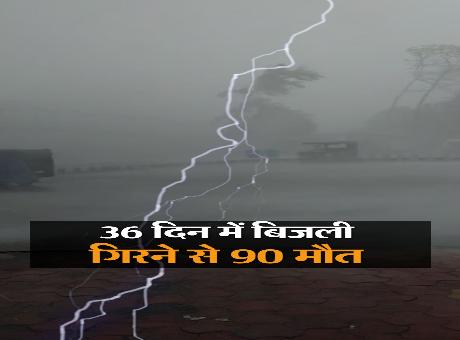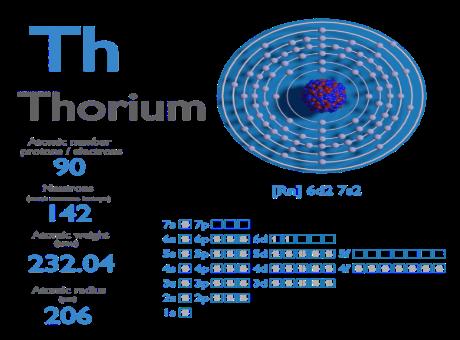भोपाल [महामीडिया] सच्चे साधु-संत भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं क्योंकि अहंकार और मोह माया को त्यागने का एक आध्यात्मिक साधन है। ''भिक्षाटन'' उन्हें सादा और संतुष्ट जीवन जीने, समाज से जुड़ाव बनाये रखने और व्यक्ति इच्छाओं से मुक्ति पाने में सहायता करता है। भिक्षा माँगने कि यह प्रक्रिया एक सामान्य भीख माँगने से अलग है। क्योंकि उद्देश्य आत्म साधना और आध्यात्मिक विकास है। एक नगर में एक संत भिक्षाटन पर नियमित रूप से जाते थे। एक माता जब भी संत के कमंडल में कुछ भोज्य पदार्थ देती तो वह सदैव संत जी से प्रवचन कहने को कहती थी परंतु वह संत सदैव उन्हें 'सौभाग्यवती' रहने का आशीर्वाद दे देते थे। कुछ समय पश्चात माता बहुत क्रोध में बोली संत महाराज में नियमित रूप से आपको यथासंभव स्वादिष्ट भोज्य पदार्थ देती हूँ और प्रवचन का आग्रह करती हूँ किंतु आप ऐसे ही चले जाते हैं। अगले दिन माता ने स्वादिष्ट खीर बनाई और भिक्षाटन पर आए संत ने जब अपना कमंडल आगे बढ़ाया तो माता ने खीर को संत के कमंडल में डालने से मना कर दिया और कहा संत महाराज आपके कमंडल में गोबर चिपका हुआ है यदि मैं इसमें स्वादिष्ट खीर डालूँगी तो यह खीर स्वादहीन व गोबर की दुर्गंध से मलिन हो जाएगी अत: आप अपने पात्र को स्वच्छ कर लें जिससे में आपको स्वादिष्ट व सुगंधित खीर दे सकूं। इस पर संत बोले माता कल आप मुझ पर क्रोधित हो रही थी कि आप मुझे कभी-भी अपने प्रवचन नहीं सुनाते माता मैं भी चाहता हूँ कि आप अपने भीतर की मलिनता का नाश कर लैं तो, मैं आपको प्रवचन सुना पाऊँगा अन्यथा उन प्रवचनों को सुनने का आप पर कुछ भी सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। माता, संत जी की बात समझ गई और उन्होंने संत जी से स्वयं को भीतर से शुद्ध व पवित्र करने का प्रयास करने का वचन दिया। हम सभी यही गलती करते हैं। बाहरी आवरण को स्वच्छ रखते हैं परंतु भीतर की मलिनता पर कोई ध्यान नहीं देते। देवी लक्ष्मी का कृपापात्र सुपात्र कौन है और कुपात्र कोन है? महाभारत के अनुशासन पर्व के ग्यारहवें अध्याय की एक कथा में स्वयं माता लक्ष्मी ने परिभाषित किया है भारतीय वांग्मय में यह कथा लक्ष्मी-रुक्मिणी संवाद के रूप में विख्यात है। वह कहती हैं- मैं ऐसे व्यक्ति में निवास करती हूँ जो निर्भीक, कार्यकुशल, कर्मपरायण, क्रोधरहित, देव आराधना को तत्पर, कृतज्ञ, जितेन्द्रिय तथा सत्वगुण से भरा हो, सेवाभावी हो, क्षमाशील हो समय व ज्ञान को जो मान दे, जो सोम्य हो, सत्य कहता हो, मन-क्रम-वचन से पवित्र हो।
देवी लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा, 'जो स्वभावत: स्वधर्मपरायण, धर्मज्ञ, बड़े-बूढ़ों की सेवा में तत्पर, मन को वश में रखने वाले, क्षमाशील तथा सामर्थ्यशाली हैं, ऐसे लोगों में मैं निवास करती हूँ।
आशय है कि... लक्ष्मी कर्म से अवश्य प्राप्त होती है, किंतु टिकती आचरण से है। लक्ष्मीवान होने के लिए मन सहित इंद्रियों को नियंत्रित रखना आवश्यक है। इन्हें साधने वाला ही बलवान और सामर्थ्यवान होकर लक्ष्मी का अर्जन कर पाता है। सबसे महत्वपूर्ण है मन का भाव। मन मैला न रखें।
लक्ष्मी कहती हैं, 'जो अपने समय को कभी व्यर्थ नहीं जाने देते, जिन्हें तपस्या एवं ज्ञान प्रिय है, ऐसे लोगों में मैं निवास करती हूँ। किंतु जिसका मन मूढ़ता से भरा है, ऐसे व्यक्ति में मैं नित्य निवास नहीं करती हूँ।'
लक्ष्मी का वचन है, 'जो स्त्रियां सत्यवादिनी, सौम्य, सौभाग्यशालिनी, पतिव्रता, कल्याणमय आचार-विचार वाली तथा सदैव वस्त्राभूषण से विभूषित रहती हैं, मैं ऐसी स्त्रियों में निवास करती हूँ। इसके उलट जो निर्दयी, धैर्यहीन, सदैव सोने वाली हों, उन्हें मैं त्याग देती हूँ।' लक्ष्मीकृपा के लिए दूसरों के प्रति दया और पवित्रता परम आवश्यक है, फिर चाहे वो स्त्री हो या पुरुष।
जो समाज अपने आसपास के वातावरण तथा जलस्रोतों के प्रति दायित्ववान होता है, उन्हें पवित्र तथा समृद्ध रखता है, लक्ष्मी उसी को अपना प्रसाद प्रदान करती हैं। ज्ञानियों और गुणियों की अधिकाधिक संख्या समाज की प्रगति, उन्नति और लक्ष्मी का ही प्रतीक है।
सार... असल लक्ष्मी तो प्रकृति है। इसके तत्वों का संरक्षक ही वास्तविक धनवान है।
हमें क्या चाहिए वह जो हमें तात्कालिक सुख दे रहा है या वह जो अंतत: आत्मा को उन्नति की ओर ले जाये। परमपूज्य महर्षि महेश योगी जी सदैव कहा करते थे कि साधु बनने के लिए हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में रहते हुए साधु बन सकता है। संयमित और आत्माभिमुख जीवन जीते हुए।
साधु मात्र बाहरी रूप धारण करने से नहीं होगा। साधुता आंतरिक गुण है। जिसका मूल है सर्वात्मक संयम। संयम का अर्थ है। अपनी इंद्रियों, विचारों और वचनों को नियंत्रित करते हुए जीवन यापन करना। इस हेतु महर्षि सदैव भावातीत ध्यान योग शैली का नियमित रूप से प्रात: एवं संध्या के समय 15-20 मिनट का अभ्यास कर आप संयमित एवं आत्माभिमुख जीवन यापन कर सकते हैं। ।।जय गुरूदेव जय महर्षि।।
[ ब्रह्मचारी गिरीश जी ]
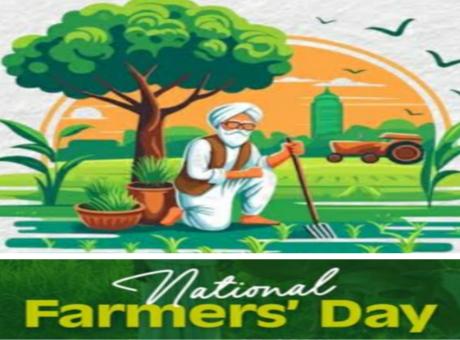 नवीनतम
नवीनतम